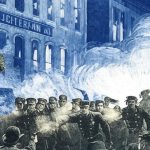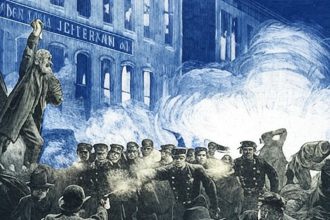महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा की विचारधारा ने दुनियाभर के जनांदोलनों और संघर्षों को प्रेरित किया है। फिर भी, इस बात की चर्चा कम ही होती है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी ने एक बड़े श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसे भारत में श्रमिक आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है।
गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके दो साल बाद 1917 में गांधी ने बिहार के चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। हुआ कुछ यूं था कि अंग्रेज शासकों के निर्देश पर जमींदार और साहूकार गरीब, भूमिहीन किसानों से जबर्दस्ती नील की खेती करवाते थे। मकसद था इंग्लैंड और यूरोप में नील की जरूरतें पूरी करना। नील की खेती से खेत बर्बाद हो रहे थे। अन्न उपजाना मुश्किल हो गया था। अंततः पीड़ित किसानों को गांधी का सहारा मिला और यह इतिहास में दर्ज है।
यह तकरीबन वही समय था, जब दुनिया प्लेग की महामारी से जूझ रही थी। भारत का बड़ा हिस्सा भी प्लेग से प्रभावित था। प्लेग ने अहमदाबाद की कपड़ा मिलों को भी प्रभावित किया, जहां प्रवासी मजदूर काम करते थे। शहर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। इससे कपड़ा मिल मालिक परेशान हो गए। श्रमिक चले जाएंगे तो उत्पादन कैसे होगा? इसकी काट उन्होंने श्रमिकों को प्लेग बोनस की पेशकश के रूप में ढूंढी। यह उनके वेतन का 75 फीसदी तक था। इसका असर भी हुआ।
तब अहमदाबाद के मिल मालिकों को प्रवासी मजदूरों की कितनी जरूरत थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर थी। आखिर अहमदाबाद को अपनी कपड़ा मिलों के कारण मैनेचेस्टर ऑफ ईस्ट यूं ही नहीं कहा जाता था। जनवरी, 1918 के आसपास जब प्लेग का असर कम होने लगा तब मिल मालिकों ने श्रमिकों को दिया बोनस और अन्य सुविधाएं वापस ले लीं। मगर श्रमिकों ने बढ़ती कीमतों का हवाला देकर वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर दी।
मिल मालिक इसके लिए तैयार नहीं थे।
अंततः श्रमिकों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुसूइयाबेन साराभाई से संपर्क किया। गजब यह है कि अनुसूइया खुद एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन थीं। इसके बावजूद वह श्रमिकों के बच्चों के लिए काम कर रही थीं। उन दिनों गांधी देशभर में घूम जरूर रहे थे, लेकिन अपना ठिकाना अहमदाबाद में बना रखा था। वकील तो वह थे ही। दस्तावेजों से पता चलता है कि गांधी को जिले के ब्रिटिश कलेक्टर की पहल पर मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी गई।
श्रमिक पचास फीसदी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक 20 फीसदी से एक पैसा अधिक देने को तैयार नहीं थे। बातचीत टूट गई और मिल मालिकों ने तालाबंदी कर दी। यह गांधी को नागवार गुजरा। अंततः मिल मालिक गांधी की पहल पर श्रमिकों के वेतन में 35 फीसदी की वृद्धि के लिए तैयार हो गए। यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला। जबकि उसी दौरान कई जगहों पर श्रमिक आंदोलनों के हिंसक होने के कई वाकये हो चुके थे।
सुब्बैया कन्नपन ने 1962 के अपने एक आलेख द गांधियन मॉडल ऑफ यूनियनिज्म इन ए डेवलपिंग इकनॉमी (आईएलआर रिव्यू) में इस पर विस्तार से लिखा है। ध्यान रहे, गांधी ने श्रमिकों की मांग को लेकर अनशन करने के साथ ही एलान किया था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वे मोटरकार में भी नहीं चलेंगे।
इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि में गांधी की मदद से अनुसूइयाबेन साराभाई ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (टीएलए) की स्थापना की थी, जो कि कई दशकों तक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन बना रहा। अनुसूइयाबेन साराभाई और गांधी के अहमदाबाद के कपड़ा मिल श्रमिकों के आंदोलन को याद करें, तो सचमुच श्रमिकों के हक में नई राह खुल सकती हैं।