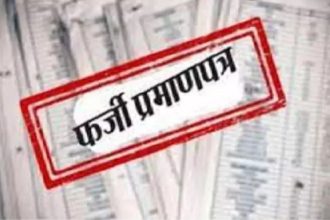भारत के Supreme Court ने 20 नवम्बर गुरुवार को 8 अप्रैल के अपने फैसले में दिए गए अपने ही निर्देश को लेकर कहा है कि राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा निर्धारित किया जाना गलत हैं और संविधान तथा शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत , न्यायमूर्ति विक्रम नाथ , न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की संविधान पीठ ने कहा कि पिछले फैसले में निर्धारित समय-सीमा और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ऐसी समय-सीमा का पालन न करने की स्थिति में विधेयकों को मान्य स्वीकृति देना, न्यायालय द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का अतिक्रमण करने के समान है और इसकी अनुमति नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं हैं लेकिन बिना वजह लंबी देरी होने पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। यह फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 संवैधानिक सवालों पर आधारित है, जो तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद से जुड़ा था।
मामला कैसे शुरू हुआ?
यह विवाद अप्रैल 2025 में तब भड़का जब सुप्रीम कोर्ट की एक दो सदस्यीय बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा रोके गए 10 बिलों को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने तब कहा था कि राज्यपाल के पास बिल रोकने की असीमित शक्ति नहीं है और उन्होंने राष्ट्रपति को भेजने का गलत फैसला लिया था। इसी फैसले में कोर्ट ने राज्यपाल के लिए एक महीने और राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की समय सीमा भी तय की थी।
इससे असहमत होकर राष्ट्रपति ने मई 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। राष्ट्रपति के सवालों में शामिल थे – राज्यपाल के विकल्प क्या हैं? क्या कोर्ट समय सीमा लगा सकता है? और क्या बिल बिना मंजूरी कानून बन सकता है? सुनवाई 19 अगस्त 2025 से चली जिसमें 8 महीने लगे।
कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच (जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रचूड़कर) ने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्यपाल के तीन विकल्प हैं – अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल बिल पर मंजूरी दे सकते हैं, विधानसभा को दोबारा विचार के लिए लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अगर विधानसभा बिल वापस भेजे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी। संविधान में समय सीमा न होने से कोर्ट इसे तय नहीं कर सकता। यह संविधान संशोधन जैसा होगा। लेकिन बिना वजह अनिश्चित देरी संघवाद के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में कोर्ट सीमित निर्देश दे सकता है।
डिम्ड असेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं: बिल को मंजूरी न मिलने पर इसे स्वत: कानून मानना गलत है। कोर्ट बिल को खुद मंजूरी नहीं दे सकता।
न्यायिक समीक्षा: राज्यपाल या राष्ट्रपति के फैसले की सामान्य समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन लंबी देरी पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति को हर बार कोर्ट की सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बेंच ने अप्रैल के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया, जो समय सीमा तय करता था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेहता ने कहा कि 1970 से अब तक सिर्फ 20 बिल राष्ट्रपति के पास लंबित रहे, जबकि 90% एक महीने में पास हो जाते हैं। लेकिन सीजेआई ने आपत्ति जताई कि आंकड़े अकेले काफी नहीं।विपक्षी राज्यों (तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल) ने केंद्र का विरोध किया। कर्नाटक सरकार की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र के प्रमुख हैं। वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं। राज्यपाल की ‘संतुष्टि’ यानी मंत्रिपरिषद की संतुष्टि।
यह फैसला केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करेगा। कई राज्य अक्सर राज्यपालों पर बिल रोकने का आरोप लगाते हैं। अब देरी होने पर राज्य सरकारें कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन समय सीमा की मांग कमजोर पड़ेगी।
द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती;
- ऐसे विधेयकों को इस आधार पर स्वीकृति नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल/राष्ट्रपति निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहे;
- किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति/राज्यपाल की कार्रवाई को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती;
- न्यायालय/न्यायिक समीक्षा के समक्ष कार्यवाही तभी होगी जब विधेयक कानून बन जाएगा;
- यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो संवैधानिक न्यायालय सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तब न्यायालय, विवेकाधिकार के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत उचित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का सीमित निर्देश जारी कर सकते हैं।
यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए संदर्भ पर सुनाया गया।
संविधान का अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है।
राष्ट्रपति के संदर्भ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य मामले में पारित 11 अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाया गया।
उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्यपालों को उचित समय के भीतर कार्य करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने के लिए संवैधानिक चुप्पी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं है।
हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 200 को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि राज्यपाल को उन विधेयकों पर कार्रवाई न करने की अनुमति मिल जाए जो उनके समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, और इस तरह राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में देरी हो और अनिवार्य रूप से बाधा उत्पन्न हो।