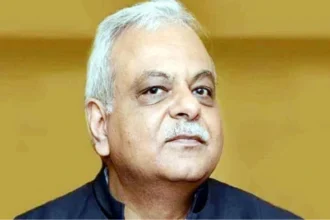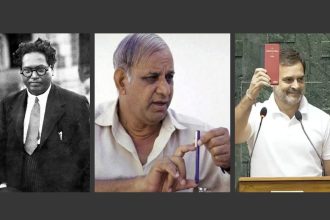भारत में सर्दियां के साथ ही असंतोष की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। मास्क मानो राष्ट्रीय गणवेश का हिस्सा बन गया है। इसे न केवल जहरीली हवाओं से अपने फेफड़ों के बचाव के लिए पहनना जरूरी है, बल्कि अपनी असहमति को छिपाने के लिए भी, ताकि मास्क के पीछे जुबान छिपी रहे। कई बार सत्ता के खिलाफ सच बोलना भारी पड़ सकता है और इसकी कीमत अस्पताल के किसी भी बिल से अधिक हो सकती है।
दिल्ली का भयावह एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक (300 से ऊपर) सुर्खियाँ बटोर रहा है और दुनिया भर में दया का पात्र बन रहा है, वहीं उन शहरों में लाखों लोग, जो शायद ही कभी बाहर निकलते हैं, लगभग खामोशी से अपने भीतर गुस्से को जज्ब कर रहे हैं।
एक मास्क खाँसी छुपाता है; दूसरा गुस्से को। दोनों ही जगहों से स्वच्छ हवा खत्म हो रही है।
वायु गुणवत्ता के मुद्दों के समन्वय, अनुसंधान और समाधान के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक 23 नवंबर, 2025 को शाम चार बजे दिल्ली के करीब स्थित बागपत में एक्यूआई 342 था, तो बहादुरगढ़ में 393, बुलंदशहर में 353, गाजियाबाद में 437, ग्रेटर नोएडा में 399 और दिल्ली में 391 था। वैसे यह इस मौसम में अब आम हो चुका है।
भारत की ज़हरीली हवा के स्रोत अलग-अलग हैं—उत्तर में पराली जलाने से लेकर बेकाबू औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों की बढ़ती संख्या और निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल तक। लेकिन नतीजा एक ही है: दम घोंटता आसमान और लड़खड़ाते फेफड़े। इसलिए विभिन्न भारतीय शहरों में खतरनाक या गंभीर AQI के कारण एक जैसे नहीं हैं।
फिर भी, भारत के वायु प्रदूषण पर तीखी बहस में, छोटे और मध्यम आकार के शहरों की दुर्दशा ज़्यादातर दबकर रह गई है, और सिर्फ़ तब सामने आती है, जब हालात चरम पर पहुँच जाते हैं। मसलन, कुछ समय पहले, असम और मेघालय की सीमा पर स्थित एक छोटा-सा औद्योगिक शहर, बर्नीहाट, भारत के नए प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में कुछ समय के लिए सुर्खियों में रहा था।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा है डाटा की कमी। भारत ने जहां वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र का विस्तार किया है, वहीं अब भी इसकी शुद्धता और निरंतरता चिंता का एक बड़ा कारण है। अध्ययन विभिन्न स्रोतों में भारी अंतक दिखाते हैं, जिससे कोई राष्ट्रीय तस्वीर नहीं बन पाती। मॉनिटरिंग स्टेशन बमुश्किल दो किलोमीटर तक की हवा की गुणवत्ता को पकड़ पाते हैं।
स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयास—जैसे मॉनिटर के पास पानी छिड़कना—शहर भर में सुधारों को दर्शाए बिना ही कृत्रिम रूप से रीडिंग कम कर सकते हैं। यह इस वास्तविकता को उजागर करता है कि शहर वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट से जूझ रहे हैं, जबकि नीतिगत ढाँचों, शोध या नागरिक सहानुभूति में इस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र का अनुमान है कि मौजूदा निगरानी ग्रिड भारत के लगभग 4,100 शहरों में से केवल 12% को ही कवर करता है। बिहार राज्य में केवल 35 निगरानी केंद्र हैं। अकेले दिल्ली में 40 हैं।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनेक छोटे और मझोले आकार के शहर वाय़ु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे यह आंकना मुश्किल है कि आखिर यह संकट है कितना बड़ा।
यहां तक कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता के मॉनिटरिंग स्टेशन हैं भी, वहां डाटा एकत्र करने में अक्सर निरंतरता नहीं दिखती, वहीं कुछ जगहो पर तो साल में 50 दिनों से भी कम की रीडिंग होती है।
शोध भी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की ओर झुका हुआ है, जिससे भिवाड़ी या बेगूसराय जैसे शहर गुमनामी में हैं। आँकड़ों के बिना, ये शहर और वहां रहने वाले लोग नीति निर्माताओं की नजरों से ओझल रहते हैं—और प्रदूषण नागरिकों की नज़रों से ओझल रहता है।
इस निराशाजनक स्थिति के बीच, कुछ ही शहर अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा का प्रबंधन कर पाए हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में PM2.5 की सांद्रता 13.8 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) दर्ज की गई है। मिजोरम के आइजोल में यह सांद्रता 16 µg/m³ है, जबकि तमिलनाडु के तिरुपुर में यह 14.8 µg/m³ है। ये शहर, जो मुख्यतः भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण में स्थित हैं, कम औद्योगिक गतिविधि, अधिक वन क्षेत्र और प्रभावी स्थानीय हस्तक्षेपों से लाभान्वित होते हैं।
छत्तीसगढ़ भी भाग्यशाली है। इस नवंबर में उत्तर भारत के किसी भी शहर की तुलना में इसके शहरों में साँस लेना ज्यादा आसान है, और यह अंतर बहुत ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ हफ्तों में जहां लगातार गंभीर AQI रहा है, रायपुर का AQI 23 नवंबर को 78 था। दुर्ग 99-110, भिलाई 64-120 के आसपास रहा और यहां तक कि कोरबा जैसे प्रदूषित औद्योगिक शहर में भी यह 78 था। छत्तीसगढ़ की हवा एकदम सही नहीं है, लेकिन यह शायद ही कभी पंजाब से उत्तर प्रदेश तक के घुटन भरे धुंध तक पहुँचती है।
राज्य का 44 फीसदी हिस्सा घने जंगल के नीचे रहता है। एक तरह से यह हरित कवच है, जो कणों को अवशोषित करता है और घातक शीतकालीन व्युत्क्रम को रोकता है। उत्तर-पूर्व से आने वाली हवाएँ पठार पर 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से बहती हैं, जो धुएं को जमने देने के बजाय उसे दूर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ धान के अवशेषों (पराली) को जलाने से उठने वाले धुएं के गुबार से बचा हुआ है।
यहां के किसान अपने मवेशियों को पराली खिलाते हैं या उससे खाद बनाते हैं; जली हुई पराली का कोई बादल दक्षिण की ओर बहकर शहरों को नहीं भरता, जैसा कि वे हर नवंबर में दिल्ली में करते हैं।
औद्योगिक नगरी भिलाई में स्थित विशाल इस्पात संयंत्र ने उत्सर्जन मॉनिटर लगाए हैं और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को डेटा भेजते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने धूल निरोधक के माध्यम से 2019 से PM2.5 में लगभग 20-25% की कुछ कमी की है। फिर भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा किए गए ऑडिट कठोर सत्य की ओर इशारा करते हैं: पुरानी कोक ओवन और भट्टियाँ अभी भी धूल उगल रही हैं, क्षणिक उत्सर्जन बच रहा है, निरीक्षण अनियमित हैं, और जुर्माना वसूलने की बजाय अक्सर धमकी दी जाती है।
यह हमें दूषित हवा के बारे में सच बोलने और आत्ममंथन की तत्काल जरूरत की ओर वापस ले जाता है। यकीनन, भारत के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन जहरीली हवा और हर समय मास्क पहनने की जरूरत एक दुखद कहानी बयां करती है। हम सभी लंबे समय तक साफ शहरों की ओर नहीं भाग सकते। हममें से ज़्यादातर लोगों के लिए यह न तो वहनीय है और न ही व्यावहारिक रूप से संभव। और इसीलिए हमें यह मांग करनी होगी कि हम जहां भी रहें, हवा साफ़ रहे।
यह दुखद है कि राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत भारत में, वायु प्रदूषण को भी पक्षपातपूर्ण नजरिये से देखा जाता है, जहां सत्ताधारी लोग पड़ोसी राज्यों या पिछली सरकारों के प्रतिद्वंद्वियों को दोष देते हैं। इससे संकट का समाधान नहीं होगा। भारत अकेला नहीं है—चीन भी जहरीली हवा से जूझ रहा है। लेकिन चीन ने 2013 में “प्रदूषण के खिलाफ जंग ” ऐलान करते हुए हजारों कोयला संयंत्रों को बंद करने, शटडाउन लागू करने और शहरों को गैस हीटिंग पर स्थानांतरित करने के बाद, सात वर्षों में पीएम 2.5 के स्तर में 40% से अधिक की भारी कमी करते हुए, इसमें भारी सुधार किया है। बीजिंग में घातक स्मॉग के दिन सालाना 200 से ज़्यादा से घटकर 10 से भी कम हो गए हैं, जिससे साबित होता है कि जब कोई देश कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो हवा तेजी से साफ़ हो सकती है।
भारत में, इतने सारे शहरों में भयावह विषाक्तता के बावजूद, वायु प्रदूषण अभी भी चुनावी मुद्दा नहीं है। राजनीतिक वर्ग यह जानता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। एयर प्यूरीफाइड वाले घरों में और मास्क के पीछे जीवन केवल अस्थायी राहत प्रदान करता है।
हकीकत यह भी है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले अधिकांश भारतीय न तो प्यूरीफायर खरीद सकते हैं और न ही घर के अंदर रह सकते हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने के अलावा विकल्प नहीं है। वायु प्रदूषण केवल बड़े शहरों की समस्या नहीं है। जहरीली हवा को नजरअंदाज़ करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है: अकाल मृत्यु, बढ़ते चिकित्सा बिल, और हमारे युवा नागरिकों का शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास अवरुद्ध। और अगर लोग दो मुखौटे पहने रहेंगे—एक जहरीली हवा के खिलाफ, दूसरा सच बोलने की कीमत के खिलाफ—तो संकट बना रहेगा।