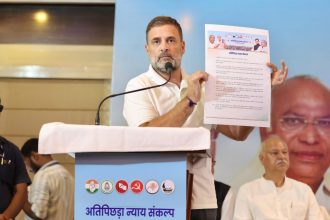छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने कल एक नवंबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो यह देखने का मौका है कि जिन उम्मीदों को लेकर इस सफर की शुरुआत की गई वह जमीन पर कितनी उतर सकी हैं।
वर्ष 2000 में जब तीन बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से अलग कर क्रमशः उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी, तो यह साफ था कि इन तीनों में छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य था, जिसकी मांग भले ही कई दशकों पुरानी रही हो, उसे लेकर उत्तराखंड या झारखंड जैसे उग्र आंदोलन नहीं हुए थे।
इसके बावजूद खनिज और वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद इस बात की संभावना थी, और आज भी है कि यह राज्य तरक्की की नई इबारत लिखेगा। शिशु मृत्यु दर और कुपोषण जैसे पैमाने पर हुए सुधार निश्चित रूप से रेखांकित करने वाले हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अब भी आश्वस्त नहीं करती।
दरअसल छत्तीसगढ़ के शहरों से लेकर गांवों तक आधारभूत पैमाने पर हुई चमक तो दिखती है, लेकिन इन वर्षों में हर जगह जिस तरह की असमानता बढ़ी है, वह चिंता का कारण होना चाहिए। मसलन इसे एक उदाहरण से ही समझा जा सकता है, नया प्रदेश बनने के समय छत्तीसगढ़ विधानसभा में 34 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं, लेकिन यह घटकर 29 हो गई हैं!
जिस प्रदेश की 32 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, उसमें उनके प्रतिनिधित्व घटने का क्या मतलब है? यही नहीं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक जिस तरह से वनाधिकार अधिनियम को कमजोर करने के प्रयास हुए हैं और ग्राम सभाओं की अनदेखी की जा रही है, वह भी किसी से छिपा नहीं है।
कुछ महीने पहले राज्य के वनविभाग को भारी विरोध के बाद अपना वह सरकुलर वापस लेना पड़ा था, जिसके जरिये वह वनाधिकार अधिनियम (एफआरआई) को कमजोर करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर अमल करना चाहता था।
कुछ समय पूर्व खुद सरकार ने संसद को बताया था कि हसदेव अरण्य में अडानी समूह की खनिज परियोजना के लिए 3.68 लाख पेड़ काटे जाएंगे। अडानी समूह महज एक दशक के भीतर ही किस तरह से बिजली क्षेत्र की सबसे दिग्गज समूह बन गया है, वह एक अलग कहानी है। लेकिन यह किस कीमत पर हो रहा है, इसे समझने के लिए यही काफी है कि अपनी स्थापना के समय जो छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली के लिए जाना जाता था, उसे आज अपनी जरूरत के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है।
केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक देश और छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्ति मिल जाएगी, और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों ने माओवादियों को जिस तरह से हाशिये पर डाल दिया है, उससे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लेकिन आगे का रोड मैप साफ नजर नहीं आता कि क्या जंगल और वन संपदा के स्वाभाविक कस्टोडियन आदिवासियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में ईमानदारी से हिस्सेदार बनाया जाएगा?
दरअसल देश के दूसरे हिस्सों की तरह इस प्रदेश में भी कॉरपोरेट के लिए लाल कालीन बिछाई जा रही हैं, इसलिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस राज्य के बनने के महज एक साल बाद 2001 में सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफा कमाने वाले भारत एल्युमिनियम लिमिटेड (बाल्को) को निजी कंपनी के हवाले कर ही दिया गया।
यह देश में किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में देने का पहला मामला था। जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कमजोर किया जाता है या उसका निजीकरण किया जाता है, तो उसका चौतरफा असर होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय को ही किसी राज्य की तरक्की का पैमाना माना जाए तो छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष प्रदेशों में कहीं नहीं है। हालांकि इससे कहीं अधिक जरूरी चीज है, रोजगार के अवसर।
बड़े उद्योग तो ठीक हैं, छोटे-छोटे कारोबारियों की सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर बड़ी कामगार आबादी के सवाल भी अपनी जगह हैं। धान के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत तो खूब हो रही है, और इससे किसानों की मोलभाव की ताकत भी बढ़ी है, लेकिन आगे का रोड मैप साफ नहीं है।
दरअसल चुनौती उन कामगारों और खेतिहर मजदूरों के लिए काम के यहां अवसर पैदा करने की है, जिन्हें हर साल महानगरों का रुख करना पड़ता है; चुनौती उस नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने की है, जिसने पहली रोशनी ही इस नए राज्य में जन्म लेने के साथ देखी थी।