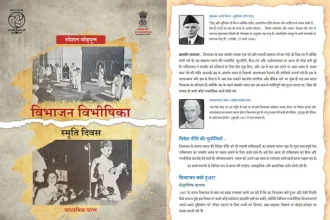नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी हाय-हाय, आज तक हाय-हाय, गोदी मीडिया हाय-हाय, पहलगाम हमले के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था में श्रीनगर पहुंचे पत्रकारों ने जब जनता से यह सवाल पूछा कि सिर्फ हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा गया है, इस पर आपका क्या सोचना है? तो जनता भड़क उठी और मीडिया के ख़िलाफ नारेबाज़ी करने लगी।
जनता अब मीडिया के सवालों पर भड़कती है, कई बार रिपोर्टर मार खा जाता है, कई बार-बाल-बाल बच जाता है। पहलगाम हमले के अगले दिन कश्मीर में ही दैनिक जागरण के पत्रकार को भाजपा के लोगों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि वह आम जनता से सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल पूछ लिए थे। बिहार के मुजफ़्फ़रपुर में बच्चों की मौत हो, नीतीश द्वारा पूर्व में भाजपा से समर्थन लिए जाने का मामला हो, सीएए-एनआरसी का प्रदर्शन हो, टीवी पत्रकार हर जगह अपमानित किए जा रहे हैं, जनता उनकी खिल्ली उड़ा रही है।

हालांकि एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार कादंबिनी शर्मा इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गलत मानती हैं। वह कहती हैं कि पत्रकारों के साथ हिंसा करना या उनकी खिल्ली उड़ाना कहीं से भी ठीक नहीं है। वह कहती हैं कि यह संभव है कि अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के काम हमें अच्छे न लगें, तो क्या हम उन्हें धमकाएंगे? हालांकि कादंबिनी यह भी मानती हैं कि डोर किसी और के हाथ में है, फजीहत पत्रकारों की हो रही है।
एक सवाल खबरों की प्रस्तुति के उत्तेजक तरीके से भी जुड़ा है। ऐसे वक्त में जब हत्या और युद्ध की खबरें रिपोर्टर नाच-नाच कर प्रस्तुत करता है, तो खबरों को लेकर उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। निस्संदेह इसकी बड़ी वजह यह है कि अब बुद्धू बक्से से जर्नलिज्म गायब है, अब जो शेष है वह सिर्फ बाजार है। जो सबसे बड़ी चीज गायब हुई है, वह है दर्शक।
टीवी चैनलों की बदली भाषा, बदले सवाल
हिंदुस्तान में देश की जनता की खबरों की भूख तब मिटी थी, जब 80 के दशक में टीवी पर नियमित खबरों का प्रसारण शुरू हुआ और दर्शक भी जुड़े। टेलीविजन एंकर जल्द ही आम जनता के हीरो बन गए। प्रसारण के तौर-तरीकों के मानक स्थापित हुए। यह कहानी बहुतों को नहीं पता है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले “आज तक” के आधे घंटे के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एस.पी. सिंह ने कमर वहीद नकवी को फोन किया और कहा कि एक समाचार बुलेटिन शुरू होने जा रहा है, उसकी भाषा तय करने का काम आप करें।

आप आज के एंकरों की भाषा देखिए, “मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो” से लेकर “मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती” या “आप थकते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी”। पहले ऐसी भाषा, ऐसे सवालों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। कई अखबारों में संपादक रह चुके वरिष्ठ साहित्यकार-लेखक विष्णु नागर जी कहते हैं कि यकीनन नफरत की भाषा बढ़ी है। मैंने तो टीवी देखना छोड़ दिया है, मुझे लगता है बहुतों ने देखना छोड़ दिया होगा। वह कहते हैं कि मैं कई बार यकीन नहीं कर पाता हूं कि जो खबर प्रस्तुत कर रहा है, यह उसकी सोच है या उसके मालिक की?
90 का दशक: टीवी पत्रकारिता का स्वर्णकाल
80 के दशक के अंत में प्रणव रॉय The World This Week नामक एक लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर आए। लेकिन 90 का दशक शुरू होते ही बाजार की धमक धीमे ही सही, सुनाई देने लगी। लेकिन टीवी पत्रकारिता के लिहाज से यह दशक शानदार था।
1975 से ही दूरदर्शन के लिए समाचार बुलेटिन बनाने वाले विनोद दुआ, प्रणव रॉय के साथ मिलकर शुरू किए गए चक्रव्यूह और करण थापर के शो की भी चर्चा हर जगह थी। 1999 में जी न्यूज ने प्राइवेट न्यूज चैनल के रूप में अपनी शुरुआत की, वहीं दिसंबर 2000 आते-आते आज तक भी शुरू हो गया। अब टीआरपी थी, रेटिंग एजेंसियां थीं।
खबरें उत्पाद में बदलीं और समाचार प्रसारण की शैली बदली। लेकिन यह बात तब भी जिंदा थी कि रिपोर्टर देश ही नहीं, दुनिया भर की खाक छानते थे। खबरों का प्रसारण स्टूडियो से होता था, खबरें स्टूडियो की बाहरी दुनिया से आती थीं। रविश कुमार, राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, मुकेश कुमार जैसे पत्रकारों ने अलग धमक दिखाई। इसी दशक में भारत के पत्रकारों ने खाड़ी युद्ध की शानदार कवरेज की। दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार की उस वक्त की कवरेज देखी जाए तो आज के दीपक चौरसिया में जमीन-आसमान का अंतर नजर आएगा।
फिर जब आया बाजार और चैनलों ने अपना ली सरकारी भाषा
मीडिया में पिछले 25 सालों से जो हुआ, वह हैरान करता है। 2008 में सामने आए नीरा राडिया टेप से मीडिया और कॉरपोरेट्स, मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के रिश्तों का खुलासा हुआ, तो पूरे देश में तहलका मच गया।
लेकिन 2014 आते-आते मीडिया खुद ही राजनीतिक पक्षधरता का शिकार हो गया। अब उसके लिए खबरें सत्ता तय करती थीं, सत्ता को खुश रखना उसका एजेंडा बन गया क्योंकि बात धंधे की थी। इसकी वजह से सबसे बड़ा पलीता खबरों को लगा। स्टूडियो में ही खबरें डेस्क पर तैयार होने लगीं। हाशिए की खबरें गायब थीं।

ग्राउंड रिपोर्टिंग इतिहास बन गई। बड़े उद्योगपतियों ने चैनल ख़रीद लिए। पत्रकारों की जगह लिपे-पुते चेहरों वाले ऐंकर और तेज-तेज चीखने और मुर्गा लड़ाई कराने वाले सूत्रधारों की भर्ती शुरू हो गई और टीवी नफरत की जादुई दुनिया में बदल गया। निस्संदेह इसके पीछे सरकारी विज्ञापन का भारी दबाव है। इन सबका नतीजा आज सामने है। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी के संपादक अतुल चौरसिया कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आक्रामक भाषा अचानक आई, जैसा कंटेंट वैसी भाषा। टीवी इंडस्ट्रीज अब घाटे का सौदा है। भूत प्रेत से शुरू होकर टीवी सत्ता की गोद में जाकर बैठ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यह जानती है कि पैसा सरकार से मिलना है तो वह उसी के अनुरूप अपने तेवर,कंटेंट और भाषा रखे हुए हैं।
हिंदी खबरें और टीवी देखने वालों की संख्या में भारी कमी
इन सबका असर यह हुआ कि देश में टीवी देखने वालों की संख्या घटती चली गई। जो सबसे उल्लेखनीय हुआ वह यह कि हिंदी कंटेंट को देखने वालों की संख्या 44 फीसदी पर पहुंच गई।
मार्केटर के अनुसार, 2023 में टीवी देखने का औसत समय 2 घंटे और 51 मिनट रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में यह 3 घंटे और 17 मिनट था। निस्संदेह यह आंकड़ा 2025 में और कम होगा।
नीलसन के डेटा से पता चलता है कि टीवी देखने वाले लोग प्रसारण टीवी की तुलना में स्ट्रीमिंग में अधिक समय बिता रहे हैं। 2022 में स्ट्रीमिंग ने एक तिहाई टेलीविजन देखने का समय हासिल कर लिया था, जो नवंबर 2022 में बढ़कर 38.5 फीसदी हो गया। ये आंकड़े अब 50 फीसदी के बराबर हैं।
टीवी न्यूज देखने वाले दर्शकों की संख्या में कमी आ रही है और स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ खबरों के नाम पर डिबेटिंग, उन्माद और नफरतगोई इसके प्रमुख कारणों में से एक है।

हालांकि, टेलीविजन अभी भी देश का सबसे बड़ा माध्यम है, जो 200 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंचता है। एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार हृदयेश जोशी का कहना है कि पहले टीवी चैनलों को यह लगा कि अगर खबरों को मनोरंजन की शैली में प्रस्तुत करेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा यह हुआ भी, लेकिन सुबह और शाम ऐसी खबरों को निरंतर देखने के बाद लोगों में एक थकान-सी आ गई।अब तो टीवी चैनल के मालिकों को भी लगने लगा है कि उनके कंटेंट देखे नहीं जा रहे हैं। इसका एक बड़ा सबूत टीवी चैनलों से भारी संख्या में पत्रकारों की नौकरी की कटौती के रूप में देखा जा सकता है।
यूट्यूब की धमक और चैनलों की अविश्वसनीयता
आज टेलीविजन समाचारों को सबसे बड़ी चुनौती यूट्यूब से मिल रही है। यूट्यूब ने पारंपरिक टीवी के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखा। 2024 में यूट्यूब 476 मिलियन भारतीयों तक पहुंच गया, जो अमेरिकी दर्शकों से दोगुना है।
यह प्लेटाफॅर्म अब टीवी के 63 फीसदी दर्शकों तक पहुंचता है, जो 2023 की तुलना में 2 फीसदी अधिक है। जो सबसे बड़ी बात हुई वह यह है कि अब जनता ने जर्नलिज्म की कमान खुद अपने हाथ में ले ली। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे हिंदी भाषी राज्यों में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से लोगों को स्थानीय भाषा में खबरें सुनने और बनाने का अवसर मिल गया।
X जैसे माध्यम ज्यादा तीव्र और सटीक सूचनाएं देने वाले साबित हुए। लोग टीवी की तुलना में सोशल मीडिया पर ज्सादा भरोसा करने लगे। टीवी चैनलों के डिबेट्स के अलावा उनका हर कंटेंट सोशल मीडिया से नदारद था।

सुप्रसिद्ध यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह इस मामले में बेहद रोचक बात कहते हैं। वह कहते हैं कि खबरें कभी मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं। जब देश में टीवी आया तो उसमें उद्योगपतियों ने भारी पैसा लगाया, उसमें भारी निवेश आया और उन्होंने ख़बरों से मुनाफा कमाने की सोची। जिसमें वह सफल हुए तो फिर जो हुआ, वह आज आपके सामने है। हालांकि श्याम यूट्यूब पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि यूट्यूब और टीवी में कोई खास अंतर नहीं है। टीवी को मीडिया मालिक तो यूट्यूब को दर्शक संचालित कर रहे हैं या बेहद संभव है कि किसी एक विचारधारा के समर्थक अच्छी खबर को गिरा दें, बुरी खबर को उठा दें।