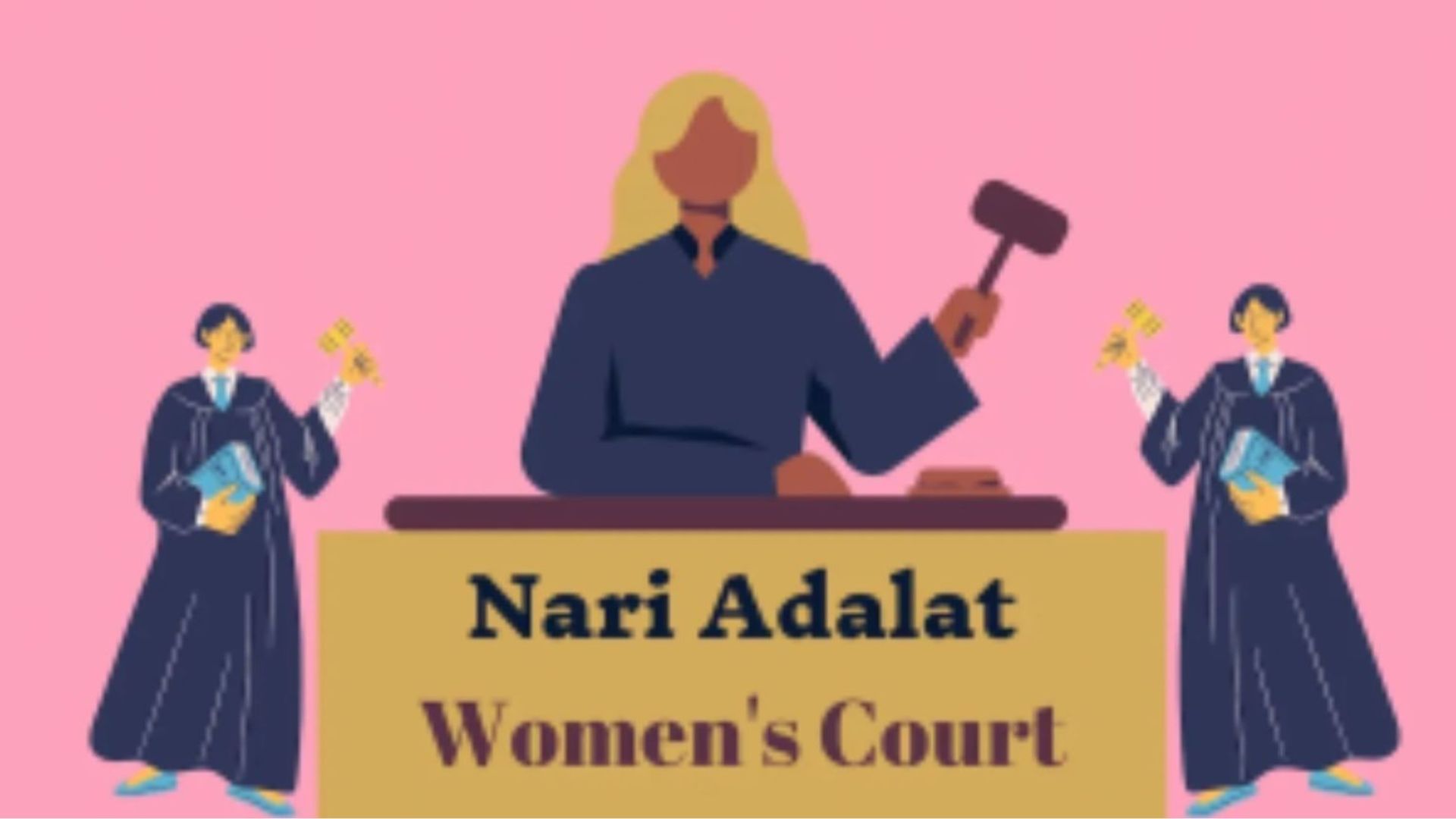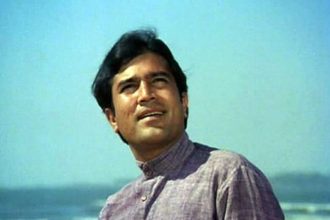भारत के शहर डूब रहे हैं। सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि नियोजन की बदतर विरासत, उपेक्षित ढांचे और उस मानसिकता में डूब रहे हैं, जो प्रकृति को सहयोगी मानने के बजाय असुविधा मानती है। अगस्त के महीने की बाढ़ ने एक बार फिर हमारे शहरी केंद्रों की कमजोरियों को उजागर किया है।
दिल्ली में इस साल दूसरी बार यमुना ने अपने किनारों को लांघ दिया। इससे निचली बस्तियां डूब गईं और हजारों लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। बंगलुरू में तो मानसून से पहले आई भारी बाढ़ ने तबाही मचाई। मुंबई पर महज चार दिनों में हुई 1000 मिलीमीटर बारिश ने कहर बरपाया, जिससे शहर का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बैठ गया और निकासी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। ये घटनाएं कोई अपवाद नहीं हैं। ये सब उस पैटर्न का हिस्सा हैं, जो गहरे संकट की ओर इशारा कर रहा है।
भारत के शहरों में बाढ़ आना अब कोई मौसमी घटना नहीं रही, बल्कि यह ढांचागत समस्या है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश तेज की है, इसके कारण समुद्र गर्म हो रहे हैं और इसने मानसून के पैटर्न को बाधित किया है। लेकिन दशकों से लापरवाही से जारी शहरीकरण ने नुक्सान को बढ़ा दिया है।

प्राकृतिक निकासी प्रणालियों को पक्का कर दिया गया है। दलदली क्षेत्रों को भर दिया गया है। झीलें कांक्रीट के नीचे दफन हो चुकी हैं। जहां कहीं तूफानी जल निकासी प्रणाली हैं, वे या तो बेकार हो चुकी हैं या आज की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं हैं।
यह कोई नई कहानी नहीं है। मुंबई में 2005 में आई बाढ़ निर्णायक मोड़ थी, या कम से कम उसे ऐसा होना चाहिए था। इसने हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और घरों, कारोबार और आधारभूत संरचना को भारी नुक्सान पहुंचाया था। मुझे याद है कि उस बारिश के थोड़े दिनों बाद मैं उस शहर में थी और मैंने पर्यावरणविद और पत्रकार (अब दिवंगत) डेरिल डी’मॉन्टे से बात की थी।
उन्होंने शहर की गलत प्राथमिकताओं की ओर इशारा किया था: हमेशा जल आपूर्ति के लिए तो कर्ज मांगा जाता है, लेकिन सीवरेज के लिए एक रुपये की भी मांग नहीं की जाती। नतीजा यह हुआ कि समुद्र से घिरे शहर में रिसने वाली सीवर लाइनों को पानी की पाइपों के समानांतर चलाया गया और न तो कचरे के और न ही स्टॉर्मवाटर के प्रबंधन के लिए कोई सुसंगत योजना बन सकी।
डी’मॉन्टे बाढ़ को लेकर बने एक कंसर्न सिटिजन कमीशन का हिस्सा थे, जिसने मुंबई के प्रभावित उपनगरों में दैनिक सुनवाई की। लेकिन समय बीतने के साथ, मीडिया का ध्यान कम हो गया यहां तक कि बाढ़ के बाद बीमारियां तेजी से बढ़ीं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, हैजा और लेप्टोस्पायरोसिस के मरीज संख्या में सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आपातकालीन चिकित्सा राहत और स्वच्छता व रोग निगरानी में मदद के लिए आगे आना पड़ा।
दो दशक बाद, 2005 के सबक पीड़ादायक रूप से प्रासांगिक हैं। हमारे शहर लगातार प्रकृति नकारने के लिए बनाए जा रहे हैं, न कि उसके साथ सहअस्तित्व में रहने के लिए। जबकि समाधान कांक्रीट नहीं, बल्कि प्रकृति में निहित है। ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (बीजीआई) एक रास्ता दिखाता है।
बीजीआई नीले तत्वों यानी जल स्रोतों (नदी, नहर, तालाब इत्यादि) के प्रबंधन को हरे तत्वों यानी वनस्पति ( पेड़-पौधे और खेत इत्यादि) से जोड़ता है। वर्षा उद्यान, बायोस्वेल (वनस्पतियुक्त गड्ढे), पुनर्जीवित दलदली क्षेत्र, पारगम्य फुटपाथ और शहरी वन बारिश के पानी को रोकते और जमा करते हैं, बहाव कम करते हैं और नालियों पर दबाव घटाते हैं। ये शहरों को ठंडा करते हैं, हवा को साफ करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं।
कुछ शहरों ने इस बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया है। बंगलुरू ने पिछले कई बरसों तक बेतरतीब फैलाव औऱ झीलों के अतिक्रमण को नजरंदाज करने के बाद इस साल की शुरुआत में ‘स्पंज सिटी’ प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य है, प्राकृतिक जल निधियों को बहाल करना, हरित कवर का दायरा बढ़ाना और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पारगम्य सतहें स्थापिक करना।
हैदराबाद का मिशन काकतीय अर्बन ने इस साल 20 से अधिक झीलों का कायाकल्प किया है, जिससे बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता और भूजल पुनर्भरण क्षमता बेहतर हुई है। चेन्नई ने पल्लीकरनई मार्शलैंड (दलदली भूमि) को पुनर्जीवित करने के काम में तेजी लाई है, यह शहर के कुछ बचे खुचे प्राकृतिक बाढ़ प्रतिरोधकों में से एक है।
मुंबई भी बीजीआई के साथ प्रयोग कर रहा है। मीठी नदी के पास महाराष्ट्र नेचर पार्क एक फलते-फूलते शहरी जंगल के रूप में विकसित हो रहा है। यह पहले एक कचरा डंपिंग ग्राउंड था। मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान ने हरित कवर और प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
लेकिन 1860 में डिजाइन की गई शहर की जल निकासी प्रणाली आज की वर्षा का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है। यहां तक कि हाई-टेक पंपिंग स्टेशन भी अगस्त में बाढ़ को रोकने में असफल रहे। और शहर के मैंग्रोव—इसकी प्राकृतिक बाढ़ रक्षा—बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से खतरे में बने हुए हैं।
दिल्ली ने बाढ़ भविष्यवाणी प्रणाली में एआई और डॉप्लर रडार की मदद से सुधार किया है और नई परियोजनाओं के लिए हरित छत और वर्षाजल संचयन को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसका निकासी संबंधी मास्टर प्लान नौकरशाही के जाल में उलझा हुआ है। शहर की स्टॉर्मवाटर संरचना वर्षा के ऐसे पैटर्न के लिए बनाई गई थी, जो अब अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण जारी है।

समस्या विचार की कमी नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। शहरी निकाय संस्थाओं के पास फंड पर्याप्त नहीं है और उनमें कर्मचारियों की भी कमी है। जलवायु संबंधी उपायों को अक्सर विलासिता समझा जाता है न कि जरूरत।
स्मार्ट सिटी मिशन में लचीलापन शामिल है, लेकिन अधिकांश शहर डिजिटल डैशबोर्ड और निगरानी ढांचे पर जोर दे रहे हैं, न कि पारिस्थितिक बहाली पर। नीति और व्यवहार के बीच भी एक चिंताजनक दूरी है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज़ के तहत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन कमज़ोर है। डेवलपर्स नियमित रूप से पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हैं, और दंड दुर्लभ हैं। अनौपचारिक बस्तियां—जहां लाखों लोग रहते हैं—बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होने के बावजूद, लचीलापन योजना से पूरी तरह बाहर हैं।
बीजीआई इस असंतुलन को दूर करने का मौका देता है। यह स्वाभाविक रूप से समावेशी, कम लागत वाला और विस्तार करने योग्य है। केरल के मीनाचिल बेसिन में नागरिक वर्षा निगरानी नेटवर्क जैसे सामुदायिक नेतृत्व वाली पहल ने दिखाया है कि हाइपरलोकल डाटा जीवन बचा सकता है। हरे-भरे बुनियादी ढांचे के डिजाइन और रखरखाव में लोगों को शामिल करने से स्वामित्व और जवाबदेही बढ़ती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि समाधान स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हों, न कि ऊपर से थोपे जाएं।
लेकिन बीजीआई के वास्तव में जड़ जमाने के लिए, भारत को शहरी पारिस्थितिक योजना के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे की जरूरत है। इसका मतलब है बीजीआई को मास्टर प्लान, ज़ोनिंग कानूनों और बुनियादी ढांचा बजट में शामिल करना। इसका मतलब है, शहरी योजनाकारों और इंजीनियरों को प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए प्रशिक्षित करना।
इसका मतलब है, दलदली भूमियों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में संरक्षित करना, न कि अतिक्रमण के लिए ज़मीन के भंडार के रूप में। और इसका मतलब है, यह स्वीकार करना कि जलवायु लचीलापन केवल अगली बाढ़ से बचने के बारे में नहीं है—यह ऐसे शहरों के निर्माण के बारे में है जो गर्म, अधिक नम और अप्रत्याशित दुनिया में फल-फूल सकें।
2025 की बाढ़ एक चेतावनी होनी चाहिए, बशर्ते कि कोई महसूस करे। हम शहरी बाढ़ को असामान्य घटना या ईश्वरीय कृत्य मानकर नहीं चल सकते। ये उस योजना प्रतिमानों का अपेक्षित नतीजा हैं, जो प्रकृति को बाधा के रूप में देखते हैं। ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है—जहां शहर सांस लेते हैं, अवशोषित करते हैं, अनुकूलन करते हैं और पुनर्जनन करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे एक ट्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि एक जरूरत के रूप में अपनाएं।
- लेखिका भारत और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर लिखने वाली स्वतंत्र स्तंभकार
इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे Thelens.in के संपादकीय नजरिए से मेल खाते हों।