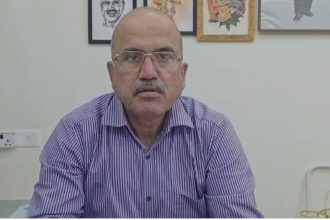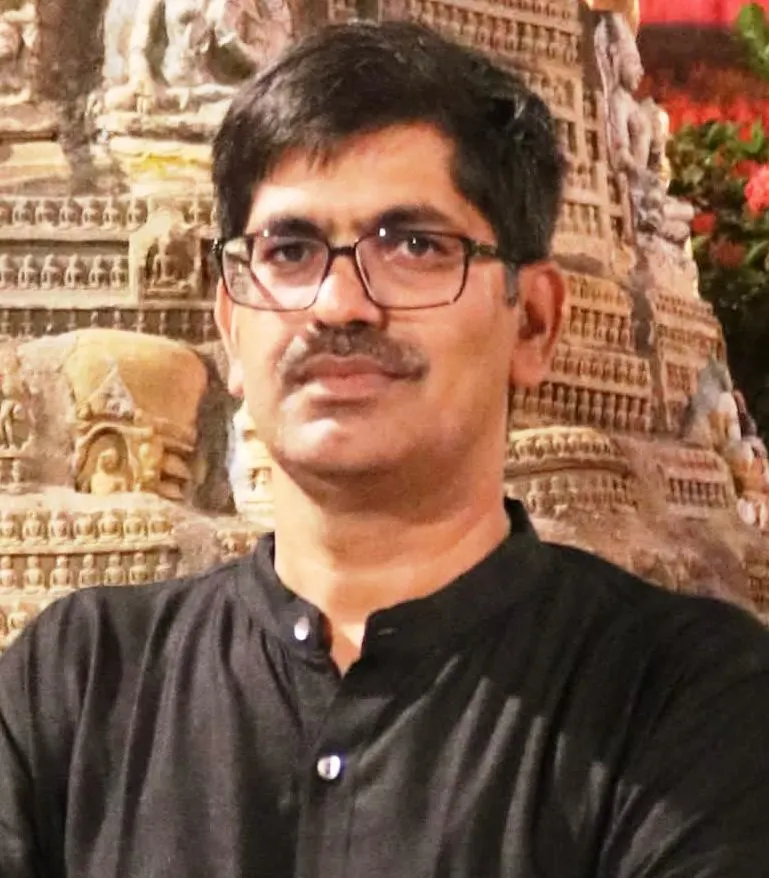
राज्य का आधार संख्या है। संख्या के बिना उसका काम नहीं चलता है। कोई चीज बिना गिने हुए छोड़ी नहीं जा सकती है। यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में गए होंगे, तो देखा होगा कि बिजली के बोर्ड, पंखे या कुर्सी आदि पर एक संख्या लिखी होती है। वस्तुओं की यह संख्या और उनका विवरण एक रजिस्टर में लिखा होता है।
सरकार या प्राधिकार की जान इन्हीं विवरणों में होती है। सरकारें अपनी जद में आने वाली हर चीज को गिनकर उसको एक श्रेणी में परिभाषित करती हैं। इससे उन्हें शासितों को सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से पुनर्विन्यस्त करने में सहायता मिलती है। जनगणना के पीछे यह तर्क काम करता है। जब से भारत में या दुनिया के किसी हिस्से में राज्य नामक संस्था का अस्तित्व है, तब से लोगों को गिना जाता है।
हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई और इसके माध्यम से उसने भारतीय जनों के बारे में एक खास किस्म के सांख्यकीय ज्ञान का निर्माण किया जिससे देश के इतने विशाल भूभाग को न केवल नियंत्रित किया जा सके बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक दायरे को ब्रिटिश शासन की चौहद्दी में कसा जा सके।
1857 के बाद मिली जातियों के पदानुक्रम को चुनौती
भारतवासियों द्वारा राजनीतिक सुधारों की माँग और ब्रिटिश शासन द्वारा उसे देने में एक आनाकानी लगी रहती थी, लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के बाद ‘संख्या बल’ एक हकीकत बन गया और उसके बाद लगभग प्रत्येक दस वर्ष पर एक नया समूह संख्याबल के आधार पर या तो डरने लगा या उसे डराया जाने लगा।
आप याद करें 1932 का एम. के. गाँधी और डॉ. बी. आर. आंबेडकर के बीच का समझौता, जहाँ समुदायों की संख्या ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ सीमित आधार पर आरक्षण दिया गया, तो उसके मूल में जनसंख्या द्वारा उत्पन्न आँकड़े थे। इस प्रकार यह आँकड़े नई उभर रही राजनीतिक चुनौतियों को सरल करने में भी प्रयुक्त किए जाते थे।
आधुनिक किस्म की पढ़ी-लिखी ‘जनता’ के निर्माण के बाद जाति और उसमें निहित पदानुक्रम को चुनौती तो 1857 के बाद ही मिलनी शुरू हो गई थी लेकिन उसे सबसे बड़ा धक्का डॉ. बी. आर. आंबेडकर के उत्थान और भारत के संविधान के निर्माण से लगा। भारत के संविधान द्वारा छुआछूत का निषेध हुआ, सबको वोट देने और जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन उस समय यह बराबरी राजनीति, शिक्षा और रोजगार में कहीं प्रकट नहीं हो रही थी।
सब जगह ऊपर की एक दर्जन के करीब उच्च जातियों के लोग ही काबिज थे।लेकिन यहाँ यह बात ध्यान रखें कि भारत के संविधान द्वारा ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिला और उसी में यह प्रावधान किया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के आरक्षण के लिए लिए सरकार को कानून बना सकती है।
1931 की गणना बनी मंडल का आधार
1950 के दशक में जब पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कालेलकर आयोग बना तो उसकी सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा नहीं माना गया। यह आयोग काल के गाल में समा गया लेकिन इस आयोग ने यह माना था कि “इससे पहले कि जाति की बीमारी को नष्ट किया जाए, इसके बारे में सभी तथ्यों को उसी तरह से एक वैज्ञानिक तरीके सेलिखना और वर्गीकृत करना होगा जैसा कि किसी ‘क्लीनिकल रिकॉर्ड’ में दर्ज किया जाता है।
इस उद्देश्य के लिए हम सुझाव देते हैं कि 1961 की जनगणना को पुनर्गठित और पुनर्नियोजित किया जाए।” इस आयोग ने जनगणना कार्य को एक सुसज्जित, निरंतर संगठन के रूप में संचालित किए जाने पर जोर दिया और कहा कि जनगणना कार्यालयों में अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त स्थायी मानवविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों को भी नियुक्त करना चाहिए।यदि सामाजिक कल्याण और सामाजिक राहत को जातियों, वर्गों या समूहों के माध्यम से प्रशासित करना है, तब तक इन समूहों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त और सारणीबद्ध की जानी चाहिए।
इस आयोग ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही थी कि जनगणना पर्चियों में अन्य विवरणों के साथ-साथ “जाति” को एक अलग कॉलम में शामिल करना चाहिए। यदि संभव हो, तो जनगणना 1961 के बजाय 1957 में की जानी चाहिए।” जैसाकि समकालीन भारत का इतिहास कहता है, इस बात को नहीं माना गया।
इसी प्रकार मंडल आयोग ने जाति जनगणना का परामर्श दिया था।1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उसने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया था कि भारत में जाति-आधारित जनगणना होनी चाहिए। ध्यातव्य है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय 1931 की जनगणना आँकड़ों का उपयोग किया था और उसे इस खामी का पता था लेकिन जब उसके पास आँकड़े नहीं थे तो भला उसके पास क्या चारा था। और यह आँकड़ों की कमी कितनी भयानक है कि जब यूपीए सरकार ने घुमंतू एवं विमुक्त जनों की भलाई के रेणके कमीशन बना तो उसने एक बार फिर 1931 की जनगणना के आँकड़ों की मदद ली।
रेणके कमीशन ने भी कहा कि जाति जनगणना हुए बिना ठीक से काम न हो सकेगा। सरकार बदली एनडीए सरकार आई। उसने इदाते कमीशन गठित किया। इस कमीशन ने भी कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इस आयोग के आँकड़ों में पूर्ववर्ती 1931 की जनगणना और रेणके कमीशन के आँकड़ों का उपयोग हुआ।यह रामकहानी दो बात बताती है कि 1931 में जाति जनगणना हुई थी और बाद की सरकारें जाति जनगणना कराने से बचती रही हैं।
1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की घोषणा ने भारतीय समाज को विक्षुब्ध कर दिया। 6 सितम्बर 1990 को भारतीय संसद में मंडल कमीशन पर हुई बहस को एक बार सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। खासकर, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजीव गाँधी, इन्द्रजीत गुप्ता, कांशीराम छबीलदास राणा और सोमनाथ चटर्जी के द्वारा की गई बहस को।
आपको पता लगेगा कि तहों के भीतर तह बनाती हुई भारतीय जाति व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तब तक क्या बातें हुई थीं। यह बहस और उसके बाद के अखबार भी दिखाते हैं कि जैसे भारत में ‘जाति प्रथा का विस्फोट’ हो गया हो। लेकिन ऐसा था नहीं।
भारतीय समाज का विशेषाधिकार संपन्न तबका यह मानने को तैयार नहीं था कि इसी भारत भूमि पर और भी लोग रहते हैं और उनकी बेहतरी आवश्यक है। वास्तव में जाति-जाति की बात करने वाला भारतीय समाज का ऊपरी मध्यवर्गीय तबका भागता रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के एक हिस्से को लागू करके उन्हें विक्षुब्ध कर दिया था।
याद रखें कि राजनेताओं को इस बात का सबसे ज्यादा भान रहता है कि वे संसद में जो बोल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। भाजपा के कांशीराम छबीलदास राणा ने मंडल कमीशन का समर्थन किया था- संसद के अंदर। इसी प्रकार राजीव गाँधी ने मंडल कमीशन का सीधे विरोध तो नहीं किया था लेकिन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किए जाने के तरीके से खुश नहीं थे। उन पर उनके विरोधियों ने सीधे तौर पर उस दिन कहा था कि जब आप सत्ता में थे इस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया था? जाहिर है कि इसका जवाब उनके पास नहीं था।
पिछले तीस-पैंतीस वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने एक करवट ली है। अब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ओबीसी को उपेक्षित करने का साहस जुटाए।नए चुनावी गठबंधनों ने इसे 1989 से प्रभावकारी बना दिया था जब अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में शामिल जातियों के बृहद चुनावी गठजोड़ों ने कांग्रेस सरकार को कभी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने लायक नहीं छोड़ा।
2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बृहद हिंदुत्व के अंदर ओबीसी जातियों के एक बड़े हिस्से को भाजपा ने समाहित कर लिया। इस तबके के समर्थन की पुनर्प्राप्ति के लिए ओबीसी आधारित पार्टियों ने न केवल अपना सामाजिक आधार विस्तृत किया है बल्कि जाति जनगणना की पुरजोर माँग की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा के साथ दलित और अल्पसंख्यक का सफल सामुदायिक गठजोड़ बनाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि जातियों को उनके अनुपात में भागीदारी मिले।उन्हें इसका सुफल भी मिला जब सपा ने 2024 के चुनाव में 37 लोकसभा सीटें जीतीं।
पिछले महीनों में कांग्रेस के राहुल गाँधी ने ईमानदार तरीके से स्वीकारा है कि कांग्रेस ने ओबीसी सहित आरक्षित वर्गों को वह महत्व नहीं दिया है जिसके वे हक़दार थे। इसी के साथ वे लोकसभा चुनाव में इण्डिया गठबन्धन में जाति जनगणना कराने और उससे भारतीय समाज का एक्सरे कराने की बात करते रहे हैं। वे भी अपने पुराने वफ़ादार मतदाताओं के साथ ओबीसी, दलित और आदिवासी राजनीति को साधना चाहते हैं।
वास्तव में, भारतीय राजनीति की ‘मेडिको-पॉलिटिकल’ भाषा से परे नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को सबसे पहले वास्तविकता में बदल दिया। उन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाई। इसी तरह कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना करवाई थी।
और जिनकी संख्या कम उनका क्या
30 अप्रैल 2025 का दिन भारत की सामाजिक राजनीति में एक यादगार दिन बन गया है। प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की जाति जनगणना करवाने की माँग मान ली है। आज मंडल आयोग की सिफ़ारिशों के लागू होने के बाद उभरे नेताओं की दूसरी पीढ़ी आ गई है और प्रत्येक राज्य में ओबीसी राजनीति ने एक स्पष्ट रूख अख्तियार किया है जिसमें प्रतिनिधित्व, सम्मान और रोजगार की लड़ाई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मोर्चों पर लड़ी जा रही है। लेकिन इसमें भी ‘भ्रंश रेखायें’ हैं।
जाति आधारित अस्मितामूलक राजनीति में जो जाति एक बार आगे चली जाती है, वह बार-बार आगे निकलना चाहती है। आज़ाद भारत में सबसे पहले इमसें तथाकथित ऊँची जातियों ने लीड ली, वह भी उसके पढ़े-लिखे हिस्से ने। अपेक्षाकृत जो सम्पन्न थे, वे विश्वविद्यालयों में गए, प्रोफ़ेसर बने, वाइस चांसलर बने। जज बने।
जजों की तो पूछिए मत, वे केवल दस-बारह जातियों से बने। इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लागू हुए आधा सदी नहीं हुआ है और उसे ठीक से लागू भी नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रक्रिया में ओबीसी जातियों का एक बड़ा हिस्सा कहीं दीख ही नहीं पड़ता है। यह जाति जनगणना उनकी संख्या को ठीक-ठीक से सबके सामने रख देगी जो सार्वजनिक जीवन में हैं और उनकी जनसंख्या भी सामने लाएगी जो ‘सरकारी दायरों’ में कहीं दिखती भी नहीं हैं।
इस जाति जनगणना को केवल ओबीसी तक नहीं महदूद किया जायेगा बल्कि इसमें दूसरे अन्य समुदाय और प्रिविलेज्ड जातियों की भी गिनती होगी। इससे यह भी दिखेगा कि भारत में ‘लोग’ किस समुदाय में हैं, सार्वजनिक जीवन में किस समुदाय के लोग हैं और यदि जमीन सहित अन्य आर्थिक आँकड़े भी जारी जारी किए गये तो यह भी दिखेगा कि भारत की आर्थिक असामनता के सामाजिक आधार कहाँ है?
जहाँ पर भूमि सुधार और आर्थिक बराबरी लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं तो उसने जाति व्यवस्था को उनके लिए अत्यधिक कष्टकारी बना दिया है। कम संख्या वाली अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग की उन जातियों का, जिनका कोई बड़ा नेता नहीं है और जो उनकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से रख सके, उनके लिए यह जनगणना एक नया मौका लायेगी। इस लेख में यह बात कही गई है कि घुमंतू और विमुक्त जनों के लिए दो-दो आयोग इसी इक्कीसवीं शताब्दी में गठित हुए। उनका कोई नामलेवा नहीं दीखता है। हो सकता है कि इस जनगणना के बाद उनके बारे में कोई सामाजिक-राजनीतिक विमर्श उभरे।
यह जनगणना इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसके आँकड़े आने के बाद सबसे पहले कार्यपालिका, न्यायपलिका और विधायिका को अपने अंत:करण में झाँकने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद 1990 के पहले और बाद के राजनीतिक दलों को अपना पार्टी संगठन दुरुस्त करना पड़ेगा। ज़ुबानी जमाखर्च के आगे उन्हें उन जातियों को प्रतिनिधित्त्व देना पड़ेगा जो अब तक इन जगहों से दूर रही हैं। इन आँकडों के आने के बाद नये जातीय इतिहास सामने आने लगेंगे। इतिहास, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के स्थापित विद्वानों को फिर से ‘फील्ड’ में जाना पड़ेगा(यदि वे जाना चाहें तो) और ठस पड़े समाज अध्ययनों को अपने को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा।
इस जनगणना में कुछ दार्शनिक और नैतिक सवाल भी निहित हैं। यह नारा लगता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें एक दिक्कत यह है कि जिसकी संख्या कम है( मैं यहाँ उच्च जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ), वे भला अपने को कैसे नियोजित करेंगे?
इस जनगणना के आने के बाद कई-कई जातियों के ‘समुदाय गुच्छ या कम्युनिटी क्लस्टर’ भी बन सकते हैं और कुछ जातियों में वे पहले से ही हैं। इन सबको मिलाकर जातियाँ अपना चुनावी गुणा-भाग करती रहेंगी लेकिन अंतिम सवाल मंशा का है। यदि कोई सरकार यह सोचे कि सबका विकास करना है लेकिन जो पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा है और जो सबसे कमजोर है, उसका विकास पहले हो तो यह सबसे बढिया बात होगी।
इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे Thelens.in के संपादकीय नजरिए से मेल खाते हों।